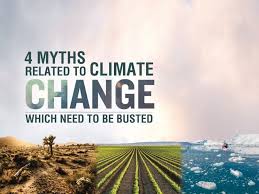
जलवायु परिवर्तन से बढ़ती दुश्वारियां Publish Date : 30/06/2025
जलवायु परिवर्तन से बढ़ती दुश्वारियां
प्रोफेसर आर. एस. सेंगर एवं डॉ0 रेशु चौधरी
जलवायु परिवर्तन की दुश्वारियों से कोई एक देश प्रभावित नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर के देश हीटवेव से जूझ रहे हैं। इसके सम्बन्ध में यदि केवल भारत की ही बात करें तो 2011 से 2022 के दशक के विभिन्न अध्यनों के अनुसार देश में हीट रिस्क दुश्वारियां और रिस्क का दायरा अधिक बढ़ गया है। मजे की बात यह है कि अब दिन को तुलना में रातें भी अधिक गर्म होने लगी है। इसका एक बड़ा कारण भवन निर्माण विधि और कंक्रीट का जंगल विकसित होना और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खासतौर से आधिक ऊर्जा खपत वाले फ्रीज और कूलर्स की जगह लेते एपरकण्डीशन भी है। घटते जंगल और आबादी का दबाव भी इसका एक बड़ा कारण है। आधुनिकता के रूप में जो संसाधान उपयोग किये जा रहे हैं वे भी जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक बन रहे हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एण्ड सीईईडब्ल्यू की हालिया रिपोर्ट अत्यधिक चिंतनीय और हालात को गम्भीरता को दर्शाती है। रिपोर्ट की माने तो देश की तीन-चौथाई आबादी आज रिस्क की जोन में आ चुकी है। देश के 734 जिलों में से 417 जिलें तो अत्यधिक जोखिम वाले जिलों में शुमार हो चुके हैं। कम जोखिम वाले जिलों में तो केवल और केवल 116 जिले ही रह गये हैं।

हालात की गम्भीरता को इसी से समझा जा सकता है कि वैसे तो हीट रिस्क के दायरें में नोर्थ ईस्ट और उत्तरी भारत के जिलों को जोड़ दिया जाए तो लगभग समूचा देश ही हॉट रिस्क के दायरें में आ चुका है। देश के दस राज्य राजस्थान, विदिशा, आन्ध्र प्रदेश, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजारात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हॉट रिस्क की अत्यधिक जद में आये प्रदेश एवं केन्द्र शासित राज्य है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही हीट रिस्क का दायरा बढ़ा है। अपितु अब यह एक वैश्चिक समस्या बन चुकी है। दुनियाभर के देशोंमें तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तेज गर्मी की तपन से हालात दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। जंगलों में दावानल र बेमौसम बरसात ऑदि तूफान, मृदा या बाबू ऐसी समस्याएं आने लगी हैं जिससे साल-दर-माल अब अधिक करना पड़ रहा है। अमेरिक का फर्नेस क्रीक सबसे अधिक गर्म स्थान है तो ट्यूनिशिया का केबिली, कुवैत का मित्रिवार, ईरान का आवाज और रेगिस्तान और चीन का फ्लेमिंग आदि स्थान ऐसे हैं जो सर्वाधिक गर्मी वाले स्थान है। इसके साथ ही मौसम के मिजाज में भी व्यापक बदलाव आया है।
सर्दियों में गर्मी और गर्मी में विभिन्न घटानएं जैसे एवं असमय आंधी, बरसात अब आम होती जा रही है और गर्मियों के दिन बढ़े हैं। फरवरी तक अब अपनी परम्परागत मौसम का दायरा छोड़ते हुए अत्यधिक गर्मी वाले महीनों में से ऐसा होने लगा है। आखिर यह मौसम का बदलाव भावी संकट की और साफ-साफ इशारा कर रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। समुद्र किनारे के शहरों के सामने उनके अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है और अब डूबने का डर सताने लगा है।
अमेरिका ही नहीं, दुनियाके अन्य देशों के जंगलों में जिस तेजी से आग की घटनाएं बड़ रही है वह अपने आप में एक अलग चुनौती बनती जा रही है। बीमारियों का असर है। हालात गम्भीर होते जा रहे हैं। हीट रिस्क के बढ़ते दायरे को देखते हुए आज हीट एक्शन प्लान बनाये जाने लगे हैं। हालांकि यदि केवल सामान्य नागरिकों के बढ़ती गर्मी के कारण होने वाले प्रभावपर ही बात की करें तो गर्मी बीमारियों का प्रमुख कारण बनती जा रही है। कई मिलियन मौतों का कारण होट वेव है।
निर्जलीकरण तो एक प्रमुख कारण तो है ही इसके साथ ही कार्डियो रेस्पिोटरी के मामलें आम होते जा रहे हैं। अनिद्रा, तनाव, सांस लेने में परेशानी, दस्त, पेट दर्द, फूड पोइजनिंग और तापघात आदि बीमारियों का प्रकोप सूतापर्क कारण दुनिया के देशों में बढ़ता जा रहा है। जिस तेजी से हीट रिस्क का बिस्तार होता जा रहा है उससे आने वाले समय में और अधिक गम्भीर हालातों का सामना करना पड़ेगा। किसी समय भारतीय परम्परा के अनुसार नौतपा एक ऐसा सभय होता था जब सबसे अधिक गर्मी पड़ती थी। यहा भी माना जाता था कि जितना अधिक नौतपा प्रभावी रहेगा उतना ही अच्छी बरसात होगी।
परन्तु आजकल यह सारे कंसेप्ट बैमानी होते जा रहे हैं। नौतपा पहले ही इतना तप चुका होता है कि एक-एक दिन निकालना भारी हो जाता है। इसके साथ ही कहीं न कहीं गर्मी मौत का या विनाश का कारण न बने इसके बारे में वैज्ञानिकों को गम्भीर मंथन करना होगा। जिस तरह से आज हमारे घर ही तापमान की वृद्धि का कारण बनते जा रहे हैं उसका कोई न कोई पर्यावरण सहयोगी साधन खोजने होंगे। पहले मकानों में चूने का उपयोग होता था तो दीपावली पर कली भी चूने की ही होती थी, परन्तु आज सारे हालात बदल गये हैं। एक तो गगनचुंबी इमारते और फिर उसका निर्माण लगे सीमेंट से और इसके साथ ही दैनिक उपयोग के तापमान बढ़ाने वाले सामानों, उपकरणों के उपयोगके चलते बहुत तापमान की नियंत्रित करने की बात करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।
ऐसें में जाम कारण चौराहों पर हरी पट्टी तान देने या सड़कों पर पानी का छिड़काव करना कोई समाधान नहीं हो सकता, बल्कि वैज्ञानिकों और नीति-नियन्ताओं को गम्भीर चिंतन करते हुए समय के रहते ही तापमान की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों को नियंत्रित करने के उपायों पर ठोस प्रयास करना होगा

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।


